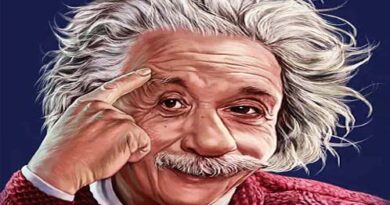क्यों न मूल शोध पर ही मिलें पीएचडी की डिग्रियां?
दिल्ली विश्वविद्यालय के हालिया संपन्न 97वें दीक्षांत समारोह में 670 डॉक्टरेट की डिग्रियां दी गईं। मतलब यह कि ये सभी पीएचडी धारी अब अपने नाम के आगे डॉ. लिख सकेंगे। क्या इन सभी का शोध पहले से स्थापित तथ्यों से कुछ हटकर था? बेशक, उच्च शिक्षा में शोध का स्तर अहम होता है। इसी से यह भी तय किया जाता है कि पीएचडी देने वाले विश्वविद्यालय का स्तर किस तरह का है। अगर अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालॉजी (एमआईटी), कोलोरोडा विश्वविद्लाय, ब्रिटेन के कैम्ब्रिज और आक्सफोर्ड विश्वविद्लायों का लोहा सारी दुनिया मानती है तो कोई तो बात होगी ही न? यह सिर्फ अखबारों में विज्ञापन देकर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्लाय नहीं बने हैं। इनका नाम उनके विद्यार्थियों द्वारा किये गये मौलिक शोध के कारण ही हैंक बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे यहां हर साल जो थोक के भाव से पीएचडी की डिग्रियां दी जाती हैं, उनका आगे चलकर समाज या देश को किसी रूप में लाभ भी होता है? सिर्फ दिल्ली विश्वविद्लाय ने एक वर्ष में 670 पीएचडी की डिग्रियां दे दीं। अगर देश के सभी विश्वविद्लायों से अलग-अलग विषयों में शोध करने वाले रिसर्चर को मिलने वाली पीएचडी की डिग्री की बात करें तो यह आंकड़ा हर साल हजारों में पहुंचेगा। मतलब हरेक दस सालों के दौरान देश में लाखों नए पीएचडी प्राप्त करने वाले पैदा हो ही जाते हैं। क्या इन शोध करने वालों का शोध भी मौलिक होता है? क्या उसमें कोई इस तरह की स्थापना की गई होती है जो नई होती है? यह सवाल पूछना इसलिये जरूरी है, क्योंकि हर साल केन्द्र और राज्य सरकारें बहुत मोटी राशि पीएचडी के लिए शोध करने वाले शोधार्थियों पर व्यय करती हैं। इन्हें शोध के दौरान ठीक-ठीक राशि दी जाती है ताकि इनके शोध कार्य में किसी तरह का व्यवधान या अड़चन न आए और इनका जीवन यापन भी चलता रहे । निश्चय ही उच्च कोटि के शोध से ही शिक्षण संस्थानों की पहचान बनती है। जो संस्थान अपने शोध और उसकी क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया जाता। देश में सबसे अधिक पीएचडी की डिग्रियां तमिलनाडू, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में दी जाती है। मानव संसाधन मंत्रालय की 2018 में जारी एक रिपोर्ट पर यकीन करें तो उस साल तमिलनाडू में 5,844 शोधार्थियों को पीएचडी दी गई। कर्नाटक में पांच हजार से कुछ अधिक शोधार्थी पीएचडी की डिग्री लेनें में सफल रहे। उत्तर प्रदेश में 3,396 शोधार्थियों को यह डिग्री मिली। बाकी राज्य भी पीएचडी देने में कोई बहुत पीछे नहीं हैं। भारत में साल 2018 में 40.813 नए पीएचडीधारी सामने आए। आखिर इतने शोध होने का लाभ किसे मिल रहा है? शोध पूरा होने और डिग्री लेने के बाद उस शोध का होता क्या है? क्या इनमें से एकाध प्रतिशत शोधों को प्रकाशित करने में कोई प्रकाशक तैयार होते हैं ? कोई प्रतिष्ठित अखबार की नजर भी उन शोधों पर जाती है ? क्या हमारे यहां शोध का स्तर सच में स्तरीय या विश्व स्तरीय होता है? यह बहुत जरूरी सवाल हैं। इन पर गंभीरता से बात होनी भी जरूरी है। जो भी कहिए हमारे यहां शोध को लेकर कोई भी सरकार या विश्वविद्यालय बहुत गंभीरता का भाव नहीं रखता । भारत में जब उच्च शिक्षा संस्थानों की शुरूआत हुई थी तभी क्वालिटी रिसर्च को बहुत महत्व नहीं दिया गया। निराश करने वाली बात यह है कि हमने शोध पर कायदे से कभी फोकस ही नहीं किया। अगर हर साल हजारों शोधार्थियों को पीएचडी की डिग्री मिल रही है तो फिर इन्हें विश्व स्तर पर सम्मान क्यों नहीं मिलता। माफ करें हमारी आईआईटी संस्थानों की चर्चा भी बहुत होती है। यहां पर भी हर साल बहुत से विद्यार्थियों को पीएचडी मिलती है। क्या हमारे किसी आईआईटी या इंजीनियरिंग के कॉलेज के किसी छात्र को उसके मूल शोध के लिए नोबेल पुरस्कार के लायक माना गया? नहीं न। अगर आप अकादमिक दुनिया से जुड़े हैं तो आप जानते ही होंगे कि हमारे यहां पर शोध का मतलब होता है पहले से प्रकाशित सामग्री के आधार पर ही अपना रिसर्च पेपर लिख देना। आपका काम खत्म। यही वजह है कि शोध में नएपन का घोर अभाव दिखाई देता है। यह सच में एक घोर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे यहां पर शोध के प्रति हर स्तर पर उदासीनता का भाव है। शोध इसलिए किया जाता है ताकि पीएचडी मिल जाए और फिर एक अदद नौकरी। आप अमेरिका का उदाहरण लें। वहां के विश्वविद्लायों में मूल शोध पर जोर दिया जाता है। इसी के चलते वहां के शोधार्थी लगातार नोबेल पुरस्कार जीत पाने में सफल रहते हैं। इस बहस को जरा और व्यापक कर लेते हैं। हमारी फार्मा कंपनियों को ही लें। ये नई दवाओं को ईजाद करने के लिए होने वाले रिसर्च पर कितना निवेश करती है? यह मुनाफे के अनुपात में बहुत ही कम राशि शोध पर लगाती हैं। यही हालत हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रही हैं। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल लिमिटेड (आईडीपीएल) की ही बात कर लें। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं में आत्मनिर्भरता हासिल करना था। पर इसे करप्शन के कारण घाटा पर घाटा हुआ। यहाँ भी कभी कोई महत्वपूर्ण शोध नहीं हुआ। अब देखिए कि भारत में शोध के लिए सुविधाएं तो बहुत बढ़ी हैं, इंटरनेट की सुविधा सभी शोधार्थियों को आसानी से उपलब्ध है, प्रयोगशालाओं का स्तर भी सुधरा है, सरकार शोध करनेवालों की आर्थिक मदद भी करती है। इसके बावजूद हमारे यहां शोध के स्तर घटिया ही हो रहे हैं। तो फिर हम क्यों इतनी सारी पीएचडी की डिग्रियों को बांटते ही जा रहे हैं? आखिर हम साबित क्या करना चाहते हैं? मैं इस तरह के अनेक शोधार्थियों को जानता हूं जिन्होंने कुछ सालों तक अपने विश्वविद्लायों से पीएचडी करने के नाम पर पैसा लिया और वहां के छात्रावास का भी भरपूर इस्तेमाल किया। उसके बाद वे बिना शोध पूरा किए अपने विश्वविद्लाय को छोड़ गए या वहीं बैठकर राजनीति करने लगे। एक बात समझ लें कि हमें शोध की गुणवत्ता पर बहुत ध्यान देना होगा। उन शोधार्थियों से बचना होगा जो दायें-बायें से कापी-कट और पेस्ट कर अपना शोध थमा देते हैं। इस मानसिकता पर तत्काल से रोक लगनी चाहिए। शोध का विषय तय करने का एक मात्र मापदंड यही हो कि इससे भविष्य में देश और समाज को क्या लाभ होगा? शोधार्थियों के गाइड्स पर भी नजर रखी जाए कि वे किस तरह से अपने शोधार्थी को सहयोग कर रहे हैं। बीच- बीच में शिकायतें मिलती रहती हैं कि कुछ गाइड्स अपने शोधार्थियों को प्रताड़ित करते रहते हैं। इन सब बिन्दुओं पर भी ध्यान दिया जाए।